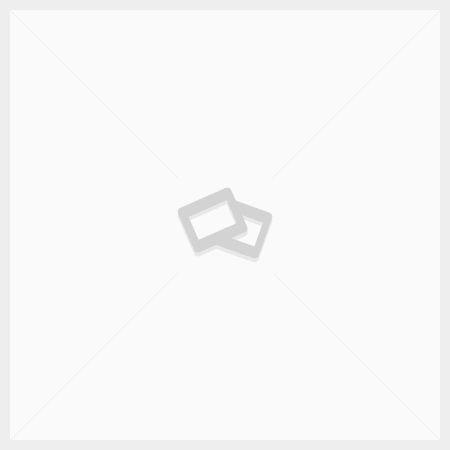किसान आन्दोलन ; अधूरी जीत को पूरी विजय में बदलना अभी बाकी है
किसान आंदोलन की निर्णायक जीत जितनी आश्वस्ति देती है उतनी – बल्कि उससे कहीं अधिक – जिम्मेदारियां आयद करती है।
भारत के अब तक के सबसे लम्बे, देशव्यापी, समावेशी और हर हिसाब से ऐतिहासिक किसान आंदोलन और उसके नतीजे में प्रधानमंत्री के खुद आकर तीन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करने और बाकी मांगों पर चर्चा का लिखित आश्वासन देने की घटना ताजा समय की एक बड़ी. उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण परिघटना है। इसे सिर्फ किसानों की समस्याओं और जिस कृषि संकट की वह उपज था ,सिर्फ उन तक सीमित रहकर समझने की बजाय ज्यादा बड़े फलक पर देखना और समझना उपयोगी होगा। इसकी शुरुआत मोटे पर इसके आम प्रभाव को दर्ज करते हुए की जा सकती है। इनमे से कुछ इस प्रकार हैं ;
पहला तो यह कि इसने निराशा तोड़ी है। सिर्फ किसानों भर की नहीं देश की समूची जनता की हताशा तिरोहित की है। नब्बै के दशक से शुरू की गयी नवउदारीकरण की नीतियां सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही कहर नहीं ढा रही थीं, इन्होने लोगों के सोचने, समझने और गतिशील होने के ऊपर भी भारी असर डाला था। यह हमला सिर्फ आर्थिक शोषण और पूँजी के वर्चस्व को पूरी तरह निर्द्वन्द तरीके से स्थापित करने भर का नहीं था। इस हमले का एक वैचारिक आयाम भी था। इसने अपनी लूट को पूरी निर्लज्जता के साथ अंजाम देने के पहले जनता पर अपना वैचारिक वर्चस्व कायम किया था। यह दो रूपों में दिखता था/है। एक तो यह कि इसने टीना (अब कोई विकल्प नहीं) फैक्टर को लगभग नियति बनाकर रख दिया। इसका विस्तार लोगों इस मानसिकता में दिखा कि ; “अब कुछ नहीं हो सकता, कि अब आंदोलन – संघर्ष वगैरा करने का कोई लाभ नहीं है।” चूंकि यह नीतियां दुनिया भर में अमल में लाई जा रही थी/हैं इसलिए यह प्रभाव भी विश्वव्यापी था।
पिछली शताब्दी की आख़िरी दहाई में दुनिया में समाजवादी व्यवस्था को लगे आघात और उसके बाद विश्व के एकध्रुवीय हो जाने ने सभी देशों की, तब तक की, अर्थव्यवस्थाओं पर एलपीजी नीतियों के रूप में विश्वबैंक, आईएमएफ, डब्लूटीओ का त्रिशूल ही नहीं घोंपा था ; एक मनोवैज्ञानिक असर भी डाला था। फ्रांसिस फुकोयामा के “इतिहास के अंत“ की,अब खुद उनके द्वारा ठुकराई गयी, थीसिस के अनुरूप गढ़े गए आख्यान की मीडिया, साहित्य, फिल्म, पाठ्यक्रमों सबके माध्यम से बमबारी की गयी। पूँजीवाद की चिरन्तरता के भरम की भरमार बौछारें की गयीं । ऐसा नहीं कि इनका असर नहीं हुआ। असर हुआ। पिछले तीस वर्षों में यदि दुनिया भर में हुयी जनता की लड़ाईयों पर सरसरी नजर डालें तो पाते हैं कि लोग अपनी मुश्किलों यानि कि परिणामो से तो लड़े किन्तु यह लड़ाई आमतौर से इसी हावी आख्यान – नैरेटिव – की सीमाओं में हुयी। मामूली राहतों के मरहम पट्टी के उपाय किये गए, वैश्वीकरण के बर्बर चेहरे पर मानवीय मुखौटा पहनाने की नाकाम कोशिशें हुईं । नीतियों के विरुद्ध उनका आक्रोश इतनी दृढ़ता और संकल्पबद्धता के साथ संघर्ष का रूप नहीं ले सका। यहां तक कि इस आक्रोश की राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ भी हुईं, जैसे लैटिन अमरीका आदि में सरकारें बदल कर नयी सरकारें बनाई गयीं किन्तु मैदानी संघर्ष या तो हुए नहीं या कम हुए ; जो भी हुए वे जितनी तीव्रता के होने चाहिए थे उतनी तीव्रता के नहीं हुए । भारत में यह धारणा मोदी के आने के बाद और मजबूत हो गयी थी। कारपोरेट-हिन्दुत्व की पारस्परिक गलबहियों वाले निज़ाम ने उनकी जो ब्रह्मा छवि बनाई ; मोदी को “जब एक बार कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर अपनी भी नहीं सुनता” जैसे सलमान खान मार्का अवतार में पेश किया – उसने बदलाव की उम्मीदों को काफी हद तक संकुचित करके रख दिया था। साल भर तक चले किसान आंदोलन ने इसे तोड़ा है। इस तरह वह हुआ है जो दुनिया में या तो हुआ ही नहीं या हुआ था तो कम ही हुआ था ।
इस तरह किसान आंदोलन ने सिर्फ बर्फ ही नहीं पिघलाई, ऊष्मा और गर्माहट भी पैदा की। इसने आम जनता का आत्मबल बढ़ाया है। लड़ाई के प्रति भरोसा पैदा किया है। यह विश्वास पैदा हुआ है कि लड़ेंगे तो नतीजे जीत में निकलेंगे। आशा की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इसके असर दिखेंगे।
दूसरा काम जो पहले से ही बहुत कठिन था, नवउदारीकरण ने और मुश्किल बना दिया था। कार्ल मार्क्स ने वर्ग विभाजित समाज में व्यक्ति के सामाजिक अलगाव के बारे में काफी नई और विचारोत्तेजक बातें बताई है। सरल भाषा में कहें तो उनका मानना था कि पूंजीवादी (सामंती भी) उत्पादन प्रणाली मनुष्य को उत्पादन प्रक्रिया का एक निरुत्साही, उचाट – डिटैच – हिस्सा बना देती है। उससे उसकी रचनात्मकता, सर्जनात्मकता छीन लेती है। उसे आत्मपरक, स्वकेन्द्रित बनाते बनाते उसकी मनुष्यता तक छीन लेती है और “कोऊ नृप होये हमें का हानि – चेरी छोड़ होय नहीं रानी “ की मंथरा अवस्था में पहुंचा देती है। उसे अपने आसपास हो रहे जुल्मोसितम, वंचनाओं के दर्द और पीड़ाओं की आहों से भी निर्लिप्त बना देती है। वर्ण और जाति, मनु, गौतम और नारद संहिताओं वाले भारतीय परिवेश में व्यक्ति का यह सामाजिक अलगाव पहले से ही भरापूरा और पूर्ण था। इस किसान आंदोलन ने, काफी हद तक, इसे भी खंडित किया है। इस आंदोलन की एक बड़ी और युगांतरकारी खासियत थी ; मेहनकशों की उस विराट एकता को कायम करना जो किसी भी सामाजिक राजनीतिक बदलाव के लिए अपरिहार्य है किन्तु न जाने कब से वह सिर्फ लिखापढ़ी तक ही सीमित थी। इस किसान आंदोलन में वह जमीन पर उतरी है। दिल्ली की सभी बॉर्डर्स पर श्रमिक कर्मचारी संगठन मेडिकल सहायता के कैम्प्स लगाए हुए थे। केरल, कर्नाटक के बैंक कर्मचारियों से लेकर रबर प्लांटेशन और काजू उत्पादन में लगे मजदूर बीसियों क्विंटल काजू, किशमिश, बादाम भेज रहे थे तो बिहार, असम, यूपी और बंगाल के कई संगठन गर्म कपड़ों, कम्बल, रजाई, गद्दे और टेंट्स की खेपें दर खेपें भेज रहे थे। संगठित मजदूरों का समर्थन सिर्फ नकदी या सामग्री की सहायता पहुंचाने भर का नहीं था । संयुक्त किसान मोर्चे के हर आव्हान को इस देश की लगभग सभी ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशनों ने अपना आव्हान माना और वे सिर्फ एकजुटता की कार्यवाही तक सीमित नहीं रहे – उससे आगे गए ।
इसी तरह छोटे दुकानदारों और छोटे मझौले कारखानेदारों की एकता भी साफ़ नुमायां थी। भागीदारी का करीब एक तिहाई महिलाओं का होना इस आंदोलन की एक और खासियत थी, जो उत्तरी भारत के जड़ सांस्कृतिक रीतिरिवाजों में महिलाओं की दशा को देखते हुए गुणात्मक रूप से नयी बात थी। । इसी तरह की एक और विशेषता इसमें युवक युवतियों, संस्कृतिकर्मियों आदि इत्यादि की हिस्सेदारी थी ।
तीसरा पहलू यह है कि इस आंदोलन के जरिये अनचाहे, अनजाने ही भारत के किसानो ने वह भूमिका निबाही है जो शास्त्रीय समझदारियों के अनुसार सामान्यतः मजदूर वर्ग निबाहता रहा है। वो इस तरह कि इसने सिर्फ अपने लिए नहीं जनता के सभी तबकों के लिए लड़ाई लड़ी है। उनकी मांगों को अपने आंदोलन के साथ जोड़ा है। कृषि कानूनों के जनता की थाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंततः देश की सम्प्रभुता तथा संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर कैसे कैसे असर होंगे यह आम भारतीयों को समझाया है और इसी दौरान चार लेबर कोड्स के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की है। यह विशिष्टता इसलिए रेखांकित किये जाने योग्य है क्योंकि गुजरी कुछ दहाईयों में प्रतिरोध का कम्पार्टमेंटलाइजेशन हुआ है ; सब अपनी अपनी मांगों के लिए अपने अपने पालों में खड़े रहकर लड़ते रहे हैं। एकजुट यलगार की कोशिशें कामुयाब नहीं हुयी हैं। इस किसान आंदोलन ने प्रतिरोध के दड़बों के बीच की सीमारेखा तोड़ने की कोशिशें की हैं तथा ऐसा करते हुए मजदूर किसान मैत्री की मजबूत बुनियाद खड़ी की है। इस तरह भारत के किसानो ने सिर्फ भारतीय कारपोरेट को ही नहीं सड़क की लड़ाईयों से साम्राज्यवाद को उसके अखाड़े – नीतियों के अखाड़े – में जाकर हराया है। इस तरह परिणामो की बजाय कारणों से लड़ने का हौंसला बढ़ाया है।
चौथा आयाम यह है कि इस आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी और उसके रिमोट कंट्रोल धारी आरएसएस और कारपोरेट के गठबंधन वाले मौजूदा निजाम की – अज्ञानी और उन्मादी बनाने की – दो जानी पहचानी धूर्तताओ को पहचाना और उसके निराविषीकरण – डेटॉक्सिफिकेशन – का काम अजेंडे पर लिया । पिछले कुछ वर्षों में आमतौर से और 2014 के बाद खासतौर से संघ-भाजपा ने भारत में रहने वाले – खासकर सवर्ण मध्यमवर्गी – मनुष्यों को उनके प्रेम, स्नेह, संवेदना और जिज्ञासा तथा प्रश्नाकुलता के स्वाभाविक मानवीय गुणों से वंचित कर दिया है। उन्हें नफरती चिंटू में तब्दील करके रख दिया है। देश के किसानो के ऐतिहासिक आंदोलन को लेकर संघी आईटी सैल के जरिये अपने ही देश के किसानो के खिलाफ इनका जहरीला कुत्सा अभियान इसी की मिसाल था । इस झूठे प्रचार को ताबड़तोड़ शेयर और फॉरवर्ड करने वाले व्हाट्सप्प यूनिवर्सिटी से दीक्षित जो शृगाल-वृन्द है उन्हें अडानी-अम्बानी या अमरीकी कम्पनियां धेला भर भी नहीं देती । इनमे से दो तिहाई से ज्यादा ऐसे हैं जिनकी नौकरियाँ खाई जा चुकी हैं , आमदनी घट चुकी है और घर में रोजगार के इन्तजार में मोबाइल पर सन्नद्ध आईटी सैल के मेसेजेस को फॉरवर्ड और कट-पेस्ट करते जवान बेटे और बेटियां हैं फिर भी ये किसानो के खिलाफ अल्लम-गल्लम बोले जा रहे थे।
इन तर्क, तथ्य और असहमति भीरुओं की बुद्धिहीनता को “हिन्दू खतरे में है“ का तूमार खड़ा करके और उन्मादी साम्प्रदायिक बनाकर असली सवालों से उसका ध्यान बंटाने का काम संघ-भाजपा- कारपोरेट ने काफी चतुराई और योजना के साथ किया। ऐसा नहीं कि इसका असर नहीं हुआ। हुआ – लेकिन किसान आंदोलन ने अपने अजेंडे पर लिया। इसके खिलाफ भी अभियान चलाया गया। आमतौर से सिर्फ आर्थिक मांगों तक सीमित रखने की समझदारी की बजाय इसने हिंदुत्ववादी साम्प्रदायिकता को मुख्य खतरा मानते हुए हर तरह की साम्प्रदायिकता को अपने निशाने पर लिया।
मगर इस सबके बाद भी यह जीत अधूरी है। मोर्चा जीता गया है युद्ध जीतना बाकी है। अधूरी इसलिए कि इससे भारत की खेती किसानी और किसानो के तुरंत जिबह होने का ख़तरा तो फिलहाल टल गया है किन्तु शनैः शनैः जारी रक्तस्राव से आसन्न मृत्यु की आशंका नहीं टली है। थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो किसान अचानक से दिल्ली बॉर्डर नहीं आये थे। कृषि संकट के खिलाफ तथा उसके वैकल्पिक समाधान को लेकर उनकी लड़ाई 2016 से जारी थी। अखिल भारतीय किसान सभा ने देश के 4 कोनों से संघर्ष सन्देश जत्थे निकालकर 24 नवम्बर 2016 को दिल्ली में एक विराट किसान रैली करके राष्ट्रीय फलक पर इसका शंखनाद किया था। इससे पहले 2014 में मोदी सरकार द्वारा लाये गए भूमि अधिग्रहण क़ानून के विरुध्द सफल संघर्ष में साझे मंच के रूप में सबसे पहले भूमि अधिकार आंदोलन अस्तित्व में आया था। इसमें 86 संगठन शामिल हैं। इसकी तरफ से दो दो संसद मार्च हुए। इसने पशु व्यापार पर रोक और उसकी आड़ में साम्प्रदायिक तथा जातीय आधार पर अल्पसंख्यकों एवं दलितों पर किये जा रहे हमलों के विरुध्द अनेक आंदोलन चलाये थे ।
इस बेचैनी और आक्रोश के देशव्यापी आंदोलन में बदलने का टर्निंग पॉइंट 6 जून 2017 को मंदसौर (मध्यप्रदेश) में किसानो पर हुआ गोलीकांड था। इसमें हुयी 6 युवा किसानों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। फसलों के वाजिब दाम तथा कर्ज मुक्ति का सवाल मुखर होकर सामने आया। इस गोलीकांड के खिलाफ सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा ने वहां जाकर हस्तक्षेप किया। सारे प्रतिबंधों को तोड़कर एआईकेएस के महासचिव हन्नान मौल्ला खुद वहां पहुंचे और बाद में इसे देश भर का मुद्दा बनाया। इसके बाद देश के अनेक किसान संगठन यहां पहुँचे , प्रायः सभी संगठनो को जोड़ा गया और इस तरह अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का साझा मंच अस्तित्व में आया जिसमे अब तक 234 संगठन सदस्य बन चुके हैं। इस संयुक्त मंच एआईकेएससीसी की तरफ से फसल के दाम तय करने के लिए स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले (लागत+लागत+50 %) अमल में लाने तथा कर्ज मुक्ति करने की मांग को लेकर मंदसौर से ही देश भर में यात्राएं निकाल कर अभियान चलाया गया , 20-21 नवम्बर 2017 में दिल्ली में किसान संसद लगाई गयी और इन दोनों कानूनों का मसविदा अपने सांसदों के माध्यम से संसद के दोनों सदनों में निजी क़ानून के रूप में रखवाया। राज्य सभा में एआईकेएस संयुक्त सचिव के के रागेश (सीपीएम) ने इसे प्रस्तुत किया। यह एकता और इसके लिए चले अभियान का प्रभाव इतना था कि 21 राजनीतिक पार्टियां दिल्ली में किसान संसद के मंच पर आईं और अपने पूर्ण समर्थन का एलान किया।
इन राष्ट्रीय स्तर की पहलों के अलावा कर्ज मुक्ति और पशु व्यापार जैसे सवालों पर किसान सभा की अगुआई में हुआ राजस्थान के किसानो का आंदोलन और नाशिक से मुम्बई तक किसानो का पैदल मार्च ऐसी बड़ी कार्यवाहियां थी जिन्होंने देश भर के किसानो को प्रेरित किया, टीना (अब कोई विकल्प नहीं है) फैक्टर से फैलाई गयी उदासी और निराशा को तोड़ा। अंततः इन सब कार्यवाहियों के जोड़ ने उस वातावरण का निर्माण किया जिसने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ इस असाधारण किसान आंदोलन और संयुक्त मोर्चा को जन्म दिया। बाकी सब ताजा इतिहास है इसलिए उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं।
इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने जो लड़ाई जीती है वह तीन कृषि कानूनों के रूप में बीच में आ गयी महाआपदा को पीछे धकेलने की लड़ाई है। असली सवाल अभी कायम हैं। इनमे सबसे बड़ा सवाल कृषि संकट उत्पन्न करने वाली नीतियों की मौजूदा दिशा को बदलने का है। वैकल्पिक नीतियां बनाने का है। दुनिया के कई देशो में ऐसा हुआ है। तर्कसंगत तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और सभी उपजों की उस दर से खरीदी की गारंटी देने वाला क़ानून बनाने , किसानो की कर्ज मुक्ति और जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्याजमुक्त दरों पर ऋण देने , कृषि के लिए आवश्यक, सिंचाई, भण्डारण, बाजार तक पहुँच आदि के लिए ढांचागत विकास में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने जैसे कदम तात्कालिक हिसाब से जरूरी हैं ; मगर स्थायी समाधान तो मौजूदा नीतियों को उलटने का ही है।
ठीक यही वजह है कि किसान आंदोलन की इस शानदार किन्तु अधूरी जीत की उपलब्धियों, इस दौरान हासिल किसानों तथा जनता की एकता को संजो कर रखा जाए और पूरी जीत हासिल करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा जोश, दमखम के साथ कमर कसी जाए। आने वाले दिन इसी तरह की जद्दोजहद के दिन होंगे।
बादल सरोज
संयुक्त सचिव अखिल भारतीय किसान सभा